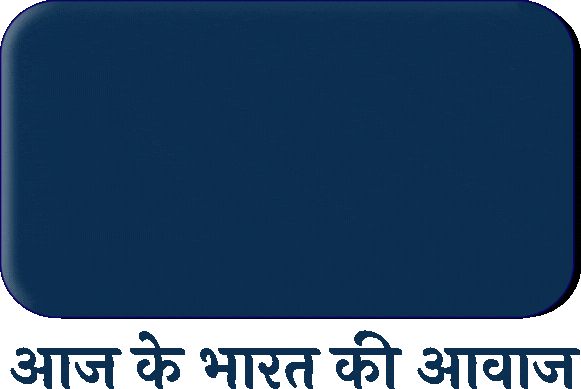Ikkis Review: बेटे की शहादत, पिता की चुप्पी, बोलती है धर्मेंद्र की खामोशी, दर्द, गर्व और इंसानियत की कहानी है 'इक्कीस'
श्रीराम राघवन की 'इक्कीस' पहली नजर में एक वॉर फिल्म लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे यह आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह फिल्म युद्ध से ज्यादा उसके असर, उसकी कीमत और उसके बाद बचे खालीपन की कहानी है। यह फिल्म गोलियों और धमाकों के जरिए देशभक्ति का शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी, यादों और अधूरे रिश्तों के जरिए बहादुरी को समझने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने 1971 के भारत–पाक युद्ध में असाधारण साहस दिखाते हुए सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त किया। 'इक्कीस' इस ऐतिहासिक घटना को सिर्फ एक युद्ध विजय की तरह नहीं देखती, बल्कि एक युवा अफसर, उसके परिवार और उसके पीछे छूट गई जिंदगी के नजरिए से पेश करती है।
दो टाइमलाइन में चलती है कहानी
'इक्कीस' की संरचना दो टाइमलाइन पर आधारित है, 1971 का युद्धकाल और 2001 का समय, जब उस युद्ध की यादें अब भी जिंदा हैं। 1971 की टाइमलाइन में हम अरुण खेत्रपाल के सैन्य जीवन, उसकी ट्रेनिंग, उसके आदर्शवाद और उस निर्णायक लड़ाई को देखते हैं जिसने उसे अमर बना दिया। वहीं 2001 की टाइमलाइन युद्ध के बाद बचे लोगों की भावनात्मक स्थिति, अधूरे सवालों और यादों के बोझ पर फोकस करती है। श्रीराम राघवन इन दोनों समय-रेखाओं को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर जगहों पर यह प्रयास सफल भी रहता है। हालांकि कुछ हिस्सों में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस होती है, खासकर सेकेंड हाफ में, जहां भावनात्मक दृश्यों की लंबाई कभी-कभी जरूरत से ज्यादा खिंचती हुई लगती है।
नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर श्रीराम राघवन, जो अपनी सधी हुई कला और विशिष्ट फिल्मोग्राफी के लिए पहचाने जाते हैं, इस बार भी निराश नहीं करते। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने सोच-समझकर उनकी उम्र के करीब के अभिनेता को चुना और उससे पूरी ईमानदारी के साथ यह किरदार निभवाया। अगस्त्य नंदा इस भूमिका में पूरी तरह डूबे नजर आते हैं और उनका अभिनय प्रभावशाली साबित होता है। यह सिर्फ एक डेब्यू परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी से निभाया गया किरदार है। अगस्त्य के साथ-साथ धर्मेंद्र भी अपनी आखिरी फिल्म में गहरी छाप छोड़ते हैं। वर्षों बाद भी वह यह साबित कर देते हैं कि उन्हें बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ क्यों कहा जाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल के पिता के रूप में उनकी परफॉर्मेंस बेहद सहज और बिना किसी बनावटीपन के है। वह दर्शकों को अपने किरदार के दर्द से जोड़ देते हैं और उसकी संवेदनाओं को पूरी ईमानदारी से सामने रखते हैं।
हर इंसान दुख से जूझने का अपना तरीका रखता है, और एक ऐसे पिता का दुख, जिसने युद्ध में अपना बेटा खो दिया हो, बेहद गहरा और जटिल होता है। धर्मेंद्र इसी जटिलता को बड़े संयम के साथ पर्दे पर उतारते हैं। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरता। वह रोते नहीं हैं, बल्कि भीतर ही भीतर टूटते हैं। उनका किरदार अपने बेटे को याद करता है, उसके आखिरी पलों को समझना चाहता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जब टैंक में आग लग गई थी और पीछे हटने का आदेश दिया गया था, तब वास्तव में क्या हुआ था। उसके मन में कई सवाल हैं, उसका बेटा क्यों नहीं लौटा, उसने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला क्यों किया?
फिल्म इक्कीस यह भी दिखाती है कि किस तरह ब्रिगेडियर नासिर (जयदीप अहलावत), एक पाकिस्तानी अधिकारी, एम.एल. खेत्रपाल (धर्मेंद्र) का बेहद सम्मान और अपनापन के साथ स्वागत करता है। पूरी ‘फौजी तहज़ीब’ के साथ उनकी मेहमाननवाज़ी की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरगोधा में उनका अपने पुराने घर का सफर संतोषजनक और यादगार बने। लाहौर लौटने के बाद ब्रिगेडियर नासिर उन्हें तीन दिनों तक अपने मेहमान के रूप में अपने साथ रखते हैं। वह नहीं चाहते कि एम.एल. खेत्रपाल किसी होटल में ठहरें, बल्कि चाहते हैं कि वह उनके घर पर रहें और कुछ दिनों के लिए उनके परिवार का हिस्सा बनें। दरअसल, फिल्म की शुरुआत ही एम.एल. खेत्रपाल की लाहौर यात्रा की योजना से होती है और समानांतर रूप से यह भी दिखाया जाता है कि ब्रिगेडियर नासिर और उनका परिवार किस तरह अपने घर में उनकी मेहमाननवाज़ी की तैयारियां कर रहे होते हैं। यह पूरा ट्रैक फिल्म को इंसानियत, सम्मान और साझा दर्द की एक गहरी परत देता है।
अभिनय
धर्मेंद्र
'इक्कीस' का सबसे भावनात्मक स्तंभ धर्मेंद्र हैं। अपने आखिरी फिल्मी किरदार में वह अरुण के पिता की भूमिका निभाते हैं और बिना किसी मेलोड्रामा के दिल तोड़ने वाला असर छोड़ते हैं। धर्मेंद्र का अभिनय बेहद सधा हुआ है। वह संवादों से ज्यादा खामोशी, नजरों और छोटे हाव-भाव से काम लेते हैं। बेटे पर गर्व, उसकी कुर्बानी का बोझ और उस खालीपन का दर्द, सब कुछ वह सहजता से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जयदीप अहलावत के साथ उनके सीन फिल्म की आत्मा कहे जा सकते हैं। दोनों के बीच होने वाली बातचीत सिर्फ दो किरदारों की नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों, दो नजरियों और एक साझा दर्द की बातचीत बन जाती है। ये सीन फिल्म को भावनात्मक ऊंचाई देते हैं, हालांकि कुछ जगह इन्हें थोड़ा और कसकर लिखा जा सकता था।
जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया
जयदीप अहलावत अपने सीमित स्क्रीन टाइम में भी प्रभाव छोड़ते हैं। उनका किरदार युद्ध की यादों को ढोते हुए एक ऐसे इंसान का है, जो आगे बढ़ चुका है, लेकिन भीतर कहीं अटका हुआ है। उनकी सहजता और संवाद अदायगी फिल्म को मजबूती देती है। सिमर भाटिया अरुण की प्रेमिका किरण के रूप में नजर आती हैं। उनका रोल छोटा है, लेकिन जरूरी है। वह उस जिंदगी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अरुण कभी पूरी तरह जी नहीं सका। हालांकि उनके किरदार को और विस्तार दिया जा सकता था, फिर भी उनकी मौजूदगी फिल्म को मानवीय स्पर्श देती है। सिमर के लुक में एक कमी नजर आती है, उनका चेहरा काफी मेच्योर है, उनकी उम्र भी असल में 27 साल है और वो 21 साल की लड़की चाहकर भी नहीं लग पातीं।
अगस्त्य नंदा
अगस्त्य नंदा का यह डेब्यू किसी भी नए अभिनेता के लिए आसान नहीं कहा जा सकता। अरुण खेत्रपाल जैसा किरदार निभाना, जिस पर पहले से इतिहास और भावनाओं का भार हो, एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगस्त्य इस चुनौती को ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन फिर कुछ कमियां रह जाती हैं। 'आर्चीज' की तुलना में उनकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार है, लेकिन अभी भी और सुधार की गुंजाइश, आर्मी अफसर के रोल में वो जोश भरने वाले एक्टर अभी नहीं बन पाए हैं। हो सकता है, उनका किरदार आपको रियलिस्टिक लगे, क्यों असल में बैटल फील्ड में फिल्मी शोर शराबा तो नहीं होता, लेकिन बॉलीवुड की जोश भरने वाली डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। उनका अभिनय बहुत ज्यादा संयमित है। वह अरुण को सुपरहीरो की तरह नहीं, बल्कि एक युवा, जिद्दी, आदर्शवादी और कभी-कभी असमंजस में पड़े अफसर की तरह पेश करते हैं। उनका किरदार अपने सीनियर्स से सवाल करता है, आदेशों को समझने की कोशिश करता है और खुद को साबित करने की बेचैनी से जूझता है। हालांकि कुछ भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय थोड़ा सपाट महसूस होता है और चेहरे के हाव-भाव और गहराई ला सकते थे, लेकिन युद्ध के दृश्यों में उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता साफ झलकती है। जलते हुए टैंक में डटे रहने वाला सीन फिल्म का सबसे प्रभावशाली पल है, जहां अभिनय, लेखन और निर्देशन एक साथ असर छोड़ते हैं।
सिनेमैटोग्रीफी
'इक्कीस' की खासियत यह है कि यह युद्ध को तमाशे की तरह नहीं दिखाती। टैंक युद्ध, बंद जगहों में फंसे सैनिक और हर पल मंडराता खतरा, सब कुछ बेहद रियल और सीमित VFX के साथ दिखाया गया है। श्रीराम राघवन यहां बड़े-बड़े स्लो मोशन शॉट्स या देशभक्ति के नारेबाजी से बचते हैं। यह फैसला फिल्म के पक्ष में जाता है, लेकिन कुछ दर्शकों को यह अप्रोच थोड़ी ठंडी भी लग सकती है। बैकग्राउंड स्कोर सधा हुआ है और कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा असर छोड़ती है। हालांकि कुछ दृश्यों में म्यूजिक और प्रभावी हो सकता था।
लेखन और निर्देशन
श्रीराम राघवन, अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सुरती का स्क्रीनप्ले भावनात्मक रूप से ईमानदार है। फिल्म बहादुरी को परिभाषित करने के बजाय उसे महसूस करने का मौका देती है। हालांकि 143 मिनट की लंबाई फिल्म को थोड़ा खींच देती है। कुछ सबप्लॉट्स को और टाइट किया जा सकता था, जिससे कहानी ज्यादा असरदार बनती। सेकेंड हाफ में फिल्म भावनाओं पर ज्यादा निर्भर हो जाती है, जहां थोड़ी काट-छांट जरूरी थी।
एक जरूरी लेकिन संयमित फिल्म
'इक्कीस' एक परिपक्व, गंभीर और संवेदनशील वॉर ड्रामा है, जो हर किसी को रोमांचित नहीं करेगी, लेकिन जो दर्शक बहादुरी के पीछे की इंसानी कहानी देखना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अहम फिल्म है। यह फिल्म याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, कुछ जंगें यादों, रिश्तों और खामोशी में भी चलती रहती हैं। अपनी कुछ कमियों के बावजूद, 'इक्कीस' ईमानदारी, भावनात्मक गहराई और सादगी के लिए देखी जानी चाहिए